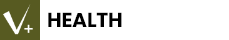* राजा जनक को ज्ञान *
एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूँ। यह सोच कर उसने एक हजार गायें मँगवाई और हरएक गाय के सींग पर बीस-बीस मोहरें बँधवा दीं और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाये, वही गायें ले जायें। एक महीने तक वाद-विवाद होता रहा। अखिर याज्ञवल्कय सब ऋषियों से अव्वल निकला और एक हजार गायें मोहरों समेत ले गया। राजा ने कहा कि मैं इसी तरह एक हजार गायें और दूँगा, जो मुझे अन्दर ले जाकर आत्म-ज्ञान करवा दे। याज्ञवल्कय वाचक ज्ञानी था। वाचक ज्ञान से सब सिद्धान्त समझा दिये, मगर ज्ञान न दे सका, अन्दर न ले जा सका। आखिर राजा ने एक सिंहासन बना दिया और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर आकर बैठ जाये। इसके बाद उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाये और कहा कि मैं उतनी देर में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जितनी देर घोड़े पर सवार होने में लगती है। ऋषि सोचते हैं कि ज्ञान कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दें। पहले कुछ लिखायें-पढ़ाये, अभ्यास कराये ंतब धीरे-धीरे कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इतने में अष्टावक्र जी आ गये। वे शरीर के टेढ़े व कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान न हुआ तो महात्मा के भेष को लाज आयेगी। यह सोच कर सिंहासन पर चुपचाप जा बैठे। उन्हें देख कर सब हँस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं समझता था कि यह महात्माओं की सभा हैं, लेकिन नहीं, ये आत्मा को नहीं देखते, ये तो शरीर को देखते हैं। शरीर को देखना तो चमारों का काम हैं सब चुप हो गये।
ऋषि ने पूछा कि राजा तू ज्ञान लेना चाहता है ? राता ने जवाब दिया कि जी हां। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, क्या देगा ? राजा ने अर्ज की, ’ जो कुछ मेरी ताकत में है, मैं आपको देने को तैयार हूँ।’ अष्टावक्र ने कहा, ’मैं भी वही माँगूंगा जोकि तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं तीन चीजें माँगता हूँ-तन, मन और धन।’ राजा ने थोड़ी देर सोच कर कहा कि मैंने दिया। अष्टावक्र ने कहा, ’ फिर सोच लो। राजा ने कहा, ’ जी मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि करो संकल्प। राजा ने संकन्प कर दिया। उन दिनों में रिवाज था कि पानी की चुल्ली भरी और संकल्प अथवा वादा हो गया। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, ’ देख राजा, तू मुझे तन, मन और धन दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतो में जाकर बैठ जा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप! अब अपनी प्रजा, अपना राज्य और सबके सामने जूतों में बैठना। मगर राजा दाना था, जरा भी न झुंझलाया। चुपचाप जूतियों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा क्यों किया ? इसलिये कि राजा की लोक-लाज छूट जाये। लोक-लाज बड़ी रुकावट है। बड़े-बड़े लोग यहाँ आकर रह जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा कि यह धन मेरा है। मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की और जाता है। फिर वापस आ जाता है। फिर वापस आ जाता है कि यह ऋषि की हैं। धन की ओर जाता है। फिर वापस आ जाता है कि यह भी ऋषि का ही है। मन की आदत है, वह बेकार और चुप नहीं बैठता, कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। इसी तरह राजा का खयाल जाता है। फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है। ऋषि देखता रहा। आखिर राजा आँखें बन्द करके बैठ गया कि मैं बाहर न देखूँ और न खयाल बाहर जाये। यही ऋषि चाहता था। अपना मतलब पूरा होता देख कर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है ? राजा जनक बोला, ’ मैं यहाँ हूँ। ऋषि ने कहा, ’ तू मन भी दे चुका है। खबरदार ! जो उससे कोई खयाल उठाया ! राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। समझने की देर थी कि मन रूक गया। जब खयाल बन्द हुआ, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जह दे दी ! रूह अन्दर चल पड़ी और रूहानी मंजिलों की सैर करने और नाम की लज्जत लेने लग गई। अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि इसको बुलाओ। अब बोले कौन ? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा, राजा को अन्दर लज्जत लेने दी। आखिर में उसका खयाल नीचे लाये। जब राजा ने आँखें खोलीं तो पूछा, क्या ज्ञान हो गया। राजा ने उत्तर दिया , जी हो गया। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक तो नहीं रहा ! जनक ने कहा, जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा, मैं यह तन, मन और धन तुझे प्रसाद के तौर पर वापस देता हूँ। अपना न समझना। राज्य भी कर और भजन भी कर। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं:
तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कउ हुकमि मंनिऐ पाईए। ( आदि ग्रन्थ्, पृ. 918 )